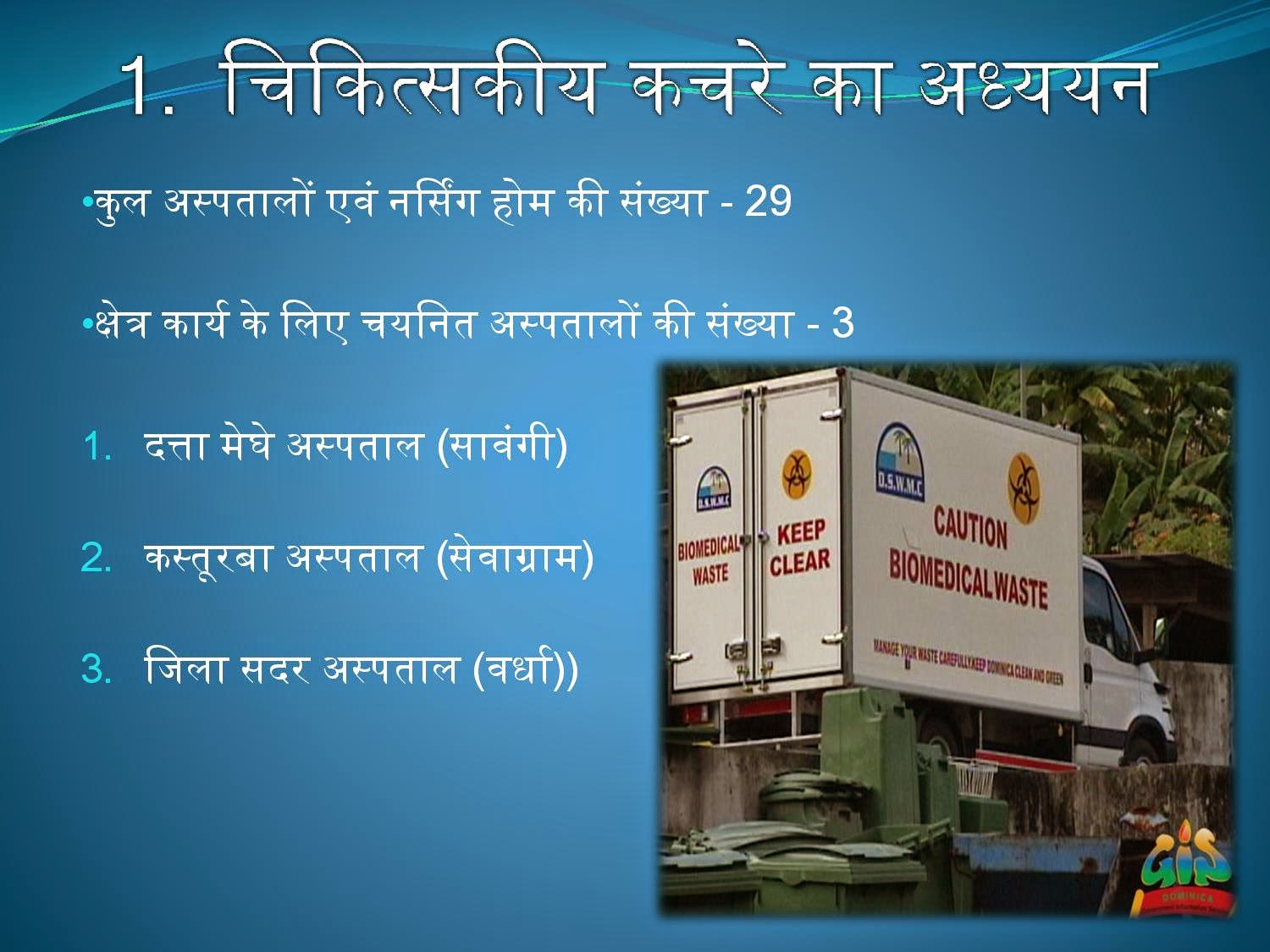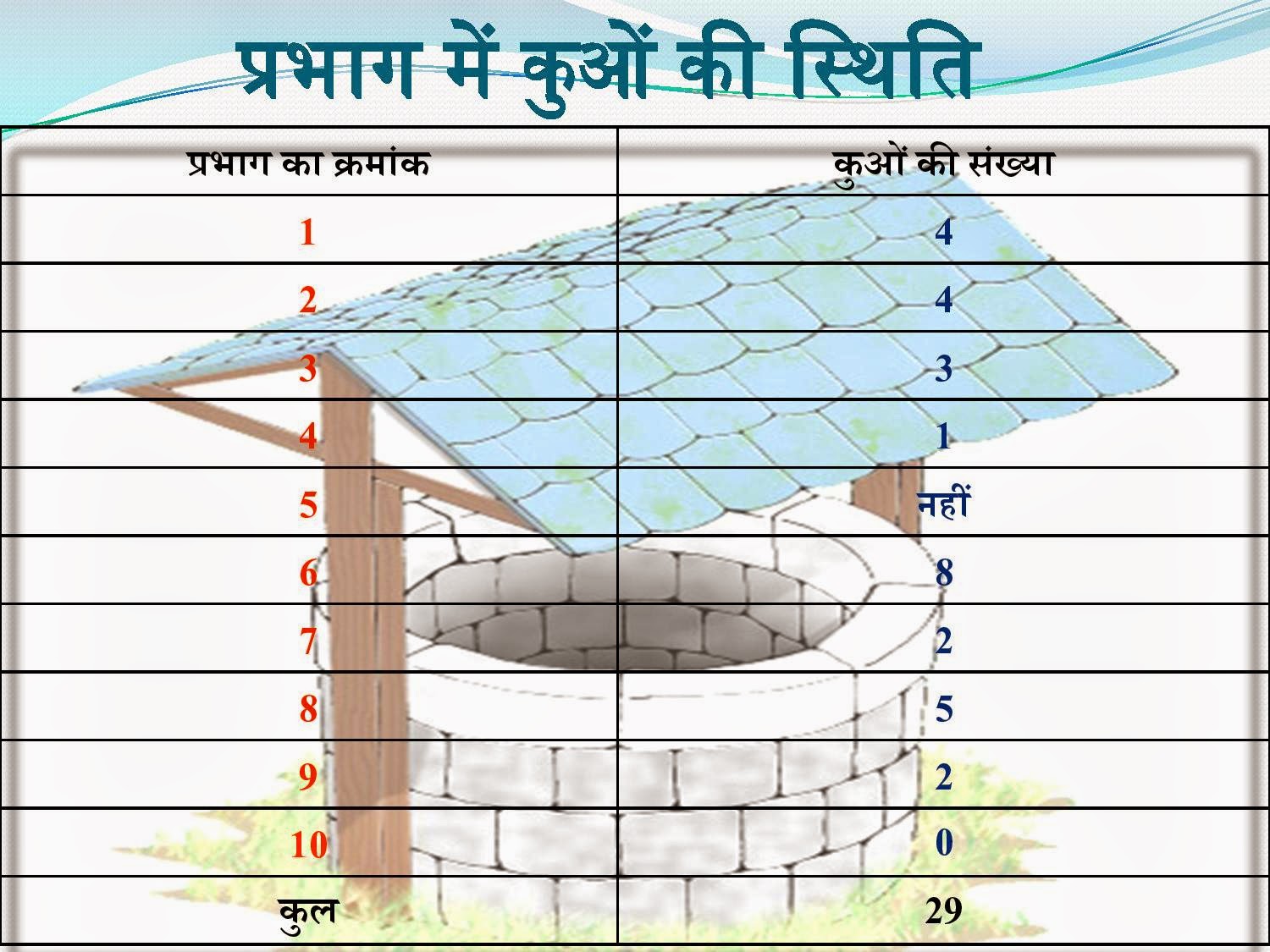मध्य प्रदेश के जिला सागर और अशोकनगर, बीना के आस पास बहुत से गाँव है, जहाँ बेड़िया समुदाय के लोग निवास करते हैं। सिर्फ एक ही गाँव जिसका नाम पथरिया है वहाँ परिवर्तन देखने को मिलता है। उसके भी कारण हैं क्योंकि वहाँ 1984 से सत्य शोधन आश्रम की शुरुआत चम्पा बेन के द्वारा की गयी जिसका मुख्य उद्देश्य बेड़िया समुदाय का उत्थान करना था।
चम्पा बेन के द्वारा सबसे पहला कार्य बेड़िया समुदाय की बालिकाओं को शिक्षा देना था और वहाँ देह व्यापार में लगी महिलाओं को जागरूक करना था ताकि वह देह व्यापार जैसे कार्य से बाहर निकल सकें। साथ ही बेड़िया समुदाय में इससे पहले शादी जैसे संस्कारों का भी कोई मूल्य नहीं था, इसके लिए भी लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। बाकी गाँव जहाँ बेड़िया समुदाय के लोग निवास करते हैं, वहाँ की स्थितियाँ बहुत ही खराब हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन राज्य की नीतियाँ भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार हैं।
बेड़िया समुदाय पहले से ही शोषित रहा है क्योंकि उनके संपर्क हमेशा राजे-रजवाड़े, जमींदारों, मालगुजारों जैसे सामन्ती लोगों के साथ रहे हैं, जहाँ लगातार उनका शोषण किया गया। जिस तरह से सामन्ती लोगों ने इनका शोषण किया उसी तरह से आज भी हो रहा है।
सरकार ने भूमिहीनों के लिए कृषि हेतु जो भूमि आवंटित की है, वह इन्हें भी आवंटित की गयी, लेकिन यह उनके निवास स्थान से 20 या 35 किलोमीटर की दूरी पर है। इनमें से बहुत सारे लोगों को आज भी उस भूमि पर कब्जे नहीं मिले हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आज तक यह भी नहीं पता है कि उनकी भूमि आखिर आवंटित कहाँ है? जब भी बेड़िया समुदाय के लोगों ने अपने आप को परम्परागत पेशे से बाहर निकालना चाहा है तो उनके सामने कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। सबसे पहला सवाल उनकी पहचान का बनता है। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि वे बेड़िया समुदाय से हैं तो लोग सहज उपलब्धता के कारण उनसे यौन संबंधो की अपील करते हैं या उन्हें उसी नजरिये से देखते हैं। इस तरह के सामाजिक दबाव को झेलना पड़ता है। यह समुदाय हमेशा किसी न किसी पर आश्रित होकर अपना जीवन निर्वाह करता रहा है। दूसरा यह समुदाय कभी कृषि कार्य से भी नहीं जुड़ा रहा। अब जिन परिवारों में दलित चेतना का विकास हुआ है और जिन्होंने अपने आप को अनुसूचित जाति की श्रेणी में भी गिनना शुरू कर दिया है, और अपने आप को इस कलंक से बाहर भी निकालना चाहते हैं, न तो उन्हें समाज इस कार्य से बाहर निकलने दे रहा है और न सरकार उनके लिए कोई ठोस कदम उठा रही है।
पूरा समुदाय हमेशा से ही उपेक्षा की नजर से देखा जाता है। यदि आप उस गाँव का नाम तक लेते हैं तो आप को लोग ओछी नजर से देखते हैं। लोगों की मानसिकता जाकर वहीं रुकती है कि आप उनके साथ अपने यौन संबंध बनाने जा रहे हैं। बुंदेलखंड में बसे ये लोग अपने लिए ही जीवन और नयी संभावनाएँ तलाश करने में जुटे तो हैं लेकिन यह सभ्य समाज ही उन्हें इस दलदल से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। दूसरा कारण यह भी है कि राज्य सरकार इनको अनुसूचित जाति की श्रेणी में श्रेणीगत करती है, लेकिन इस समुदाय में आज भी वह चेतना नहीं जागी है। यहाँ तक कि बहुत से बेड़िया आज भी अपने को उच्च श्रेणी में ही गिनते हैं। ये उन लाभों को भी नहीं ले पाते हैं, जो सरकार अनुसूचित जाति के लिए देती है। पूरे समुदाय में शिक्षा की कमी भी इनके विकास में सबसे बड़ी अवरोधक है, जो इन्हें इस काम से बाहर नहीं निकलने दे रही है।
यदि पूरे बुंदेलखंड और उसकी परिस्थितियों को देखेँ तो ये भी कृषि के लिए अनुकूल नहीं है। जब इनके इतिहास पर नजर डालते हैं तो यह समुदाय कभी भी कृषि कार्य या अन्य व्यवसाय से जुड़ा दिखायी नहीं देता है। अतः इनके लिए कृषि कार्य से जुड़ना अपने आप में एक मुश्किल कार्य है। जिस तरह से इस समुदाय कि निर्मिति के साक्ष्य मिलते हैं उससे तो यही लगता है कि इस समुदाय के उत्थान के लिए सरकार या अन्य संस्थायें इनको इस देह व्यापार के व्यवसाय से बाहर निकालना नहीं चाहती हैं, अन्यथा इनके लिए किसी उचित व्ययसाय की व्यवस्था की जानी चाहिए थी।
ग्राम परसरी की बेला कहती हैं कि- “मुझे यह काम छोड़े काफी साल हो गए हैं। अभी तक मेरा पूरा परिवार इस काम से बाहर आ गया है लेकिन जब से हमने देह व्यापार और राई को छोड़ा है, तब से हम लोग अपने लिए रोजी-रोटी का जुगाड़ भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। हमारे ही गाँव के लोग आज हमसे बहुत धनी हैं और उनके पास आधुनिक सुख सुविधा के साधन हैं, रहने के लिए अच्छे घर हैं। हम तो रोटी के लिए भी मोहताज हैं, बीड़ी बनाने और मजदूरी से घर का खर्च तो किसी तरह चल जाता है लेकिन किसी और काम के लिए पैसे नहीं बचते हैं। कई बार तो यही लगता है कि हमने राई को छोड़ कर बहुत गलत किया। कई बार वापस जाने का मन भी करता है लेकिन फिर सोच कर रह जाती हूँ ”।
यह कहानी किसी एक महिला की नहीं है। बेड़िया समुदाय में इस तरह के बहुत से परिवार मिल जाएंगे। करीला की एक महिला बताती हैं कि सामाजिक दबाव के चलते मैंने राई तो छोड़ दी, लेकिन कोई और काम भी नहीं था। घर के मर्द कुछ भी नहीं करते और पूरे दिन दारू के नशे में घूमते हैं। दारू के लिए भी पैसे मुझसे ही माँगते हैं, इसलिए वापस यहाँ करीला मंदिर पर ‘बधाई’ करती हूँ। शाम तक 2-3 सौ रुपए मिल जाते हैं पर कभी-कभी कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन अपने साथ साज वाले को रोज पैसे देने पड़ते हैं। यह किस्सा किसी एक महिला का नहीं है ऐसे किस्सों से बेड़िया समुदाय भरा पड़ा है।
बेड़िया समुदाय की पहचान एक यौन कर्म करने वाले समुदाय के रूप में सभ्य समाज करता है, लेकिन किसी भी समुदाय और उसके व्यवसाय को समझने के लिए, उस समुदाय की निर्मिति एवं इतिहास को देखना आवश्यक है, क्योंकि बिना किसी की निर्मिति के बारे में जाने उसके बारे में ठीक-ठीक कुछ कहना मुश्किल हो जाता है या कई बार हम उनके लिए गलत निर्णय भी ले लेते हैं। बेड़िया समुदाय को राज्य एक वेश्यावृत्ति करने वाला समुदाय मानता है। क्योंकि यह समुदाय अपने सेक्सुअल रिलेशन कई पुरुषों और सभ्य समाज के संबंधों से इतर बनाता है और उन संबंधो में काफी खुलापन भी होता है। यह समुदाय इस तरह के संबंध बनाने को बुरा नहीं मानता। लेकिन राज्य की विधि और सभ्य बनाने की जो राज्यजनित अवधारणा है, यह समुदाय एक ख़तरे के रूप में उसके सामने खड़ा है। जब इस समुदाय में कभी भी यौन कर्म को बुरा नहीं माना गया और समुदाय यौन कर्म को मान्यता भी देता है, तो उस समुदाय को यह सभ्य समाज या राज्य बुरा कर्म करने वालों की नजर से क्यों देखता है? जब कि इनकी संस्कृति का यह एक अहम हिस्सा भी है। यदि इनके पूरे इतिहास को देखा जाए तो यह एक घुमंतू समुदाय रहा है और कभी भी शादी-ब्याह जैसे संस्कारों को मान्यता न देते हुये अपना विकास करता रहा है। इस समुदाय के लिए यह एक सहज प्रक्रिया है लेकिन राज्य और समाज की नजर में तो नहीं।
राज्य इस तरह के समुदाय को मुख्य धारा में लाने के प्रयास में लगा है, क्योंकि यह समुदाय मुख्य धारा के विपरीत अपने संबंध मुख्य धारा के लोगों के साथ ही स्थापित करता है। लेकिन वही समाज जो इन्हें अपनी रखैल या जो भी नाम दिया जाए के रूप में इस्तेमाल करता है तब ये बेड़िया उनके लिए असभ्य क्यों नहीं होते? यही वो सभ्य समाज है जो इन्हें वेश्यावृत्ति करने वाला भी कहता है और इन्हीं के साथ अपने अनैतिक संबंध भी स्थापित करता है।
समुदाय की निर्मिति में सामन्ती लोगों की भूमिका अधिक दिखायी देती है क्योंकि ऐतिहासिक तथ्यों को देखें तो बेड़िया समुदाय की महिलाएँ राजे-रजवाडों और सामन्ती लोगों से ही अपने संबंध बनाती दिखती हैं। इसका यह कारण भी था कि बेड़िया समुदाय की महिलाएँ अन्य समुदायों की अपेक्षा अधिक सुंदर होती थीं तो इन्हें अन्य समुदायों की अपेक्षा ख़तरे भी अधिक थे। अपने संरक्षण और आर्थिक जरूरतों को पूर्ण करना भी इसमें शामिल था। यहाँ तक इनके सामने कोई समस्या नहीं थी। ब्रिटिश काल में इन्हें पहचान कर, श्रेणी बद्ध किया गया और अपराधी प्रवृत्ति की संज्ञा दी गयी। लेकिन आजादी के बाद से इनके लिए संकट बढ़ गए। उसके कारण यह थे कि भारत के लगभग सभी ऐसे समुदायों को मुख्य धारा में लाने के लिए जनजाति से जाति व्यवस्था में लाना था क्योंकि राज्य की सत्ता जाति व्यवस्था पर चलती है। इसमें शामिल होने के लिए आप को जाति व्यवस्था में आना पड़ेगा। इनके साथ भी वही किया गया। इन्हें अब जनजाति से बदल कर अनुसूचित जाति में परिवर्तित कर दिया गया। अब जब यह जाति व्यवस्था में आ चुके थे, तो राज्य की विधि के अनुसार ही इन्हें भी चलना था।
हालांकि समुदाय में खुले तौर पर संबंध बनाने की छूट थी। इसी आधार को देखते हुये राज्य ने इन्हें वेश्यावृत्ति करने वाले समुदाय के रूप में पहचान दी। औपनिवेशिक मानसिकता के साथ इन्हें शिक्षित करने की प्रक्रिया और उनकी संस्कृति को समाप्त करने के प्रयास शुरू किए गए। अब इनके सामाजिक मूल्यों, इनकी संस्कृति सभी पर हमला होना तय था। अब इन्हें ‘Open Relation रखने वाले समुदाय या व्यक्ति कभी सभ्य नहीं हो सकते’ इस मानसिकता के साथ सभ्य बनाने के लिए शिक्षित करना था। लेकिन यहाँ एक बात सबसे जरूरी हो जाती है कि इस राष्ट्र-राज्य की अवधारणा में जहाँ इस तरह के समुदाय (बेड़िया समुदाय) जो शादी ब्याह जैसे संस्कारों और सभ्य समाज के बनाए मूल्यों से अलग थे, जो किसी भी पुरुष से अपने स्वच्छंद संबंध बना सकता था, जब राज्य उसे वेश्या का संबोधन दे रहा है तब उसने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि इनके लिए आखिर ग्राहक कहाँ से आ रहें हैं? जो राज्य इन्हें वेश्या का संबोधन दे रहा है दरअसल वही राज्य ही इन्हें ग्राहक भी उपलब्ध कराने का कार्य करता है। अभी तक जिन भी संस्थाओं ने इनके लिए काम करने शुरू किए, वे सभी इन्हें सभ्य समाज की धारा में लाना चाहते हैं। आखिर एक ऐसा समुदाय जो अपने आप को अलग रखकर स्वच्छंद रहता है, किसी से भी अपने संबंध स्थापित करता है और अपने किसी भी निजी मामले में बंधन नहीं रखता, तो उन्हें बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? लेकिन जिन भी संस्थाओं ने इनके उत्थान के लिए काम शुरू किये, वे भी इन्हें राज्य की नजर से ही देखते रहे।
जब हम इन्हें सभ्य बनाने की बात करते हैं तो हम उन्हें खुद संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में ला रहे हैं। लेकिन कार्य के आधार से समुदाय की पहचान को देखें तो राज्य उन्हें निम्न श्रेणी में ही श्रेणीबद्ध करता है। तो जाहिर सी बात है एक जाति से उठकर यदि वह दूसरी नीची जाति में प्रवेश करते है तो इनके लिए संकट और बढ़ जाते हैं।
राज्य की भूमिका पर गौर किया जाए तो राज्य जहाँ एक तरफ वेश्यावृत्ति को खत्म करना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं जगहों को पहचान कर जहाँ वेश्यावृत्ति होती है, वहाँ एड्स जैसे प्रोग्राम चला कर, घर-घर में condom बाँट रहा है, यानि राज्य उन्हें संरक्षण देता हुआ प्रतीत होता है। दूसरी तरफ समुदाय के साथ व्यवहार का रवैया मुख्य धारा की मूल्य व्यवस्था (value system) से मिलता हुआ दिखयी देता है। The Hindu[1] में छपी एक रिपोर्ट को यदि देखा जाए तो राम सनेही जो एक समाज कार्यकर्ता हैं, वह इसे अनैतिक बताते हैं और बेड़िया समुदाय की परंपराओं को खत्म करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। जब कि सरकार की तमाम एजेंसियां इन्हें संरक्षण दे रही हैं। मुख्य धारा की मूल्य व्यवस्था के आग्रह वाले राम सनेही अकेले नहीं हैं, बल्कि अन्य कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थायें भी इसमें संलग्न हैं। कुल मिला कर बेड़िया समुदाय की यौनिकता समाज और राष्ट्र-राज्य के विरोधाभासी दबाव का शिकार बनती है। जहाँ एक तरफ राष्ट्र-राज्य समुदाय की यौनिकता को अपनी यौनिक अर्थव्यवस्था के तहत बचाए भी रखना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ मुख्य धारा के समाज के नैतिक और सांस्कृतिक आग्रहों को ख़ारिज भी नहीं करना चाहता। ये संस्थायें अपने सामुदायिक कार्यों में बेड़िया समुदाय के साथ सांस्कृतिक राजनीति की एजेंट दिखाई देती हैं।
समुदाय यौनिकता के संस्कृतिकरण की प्रक्रिया खास संदर्भों में घटित होती है, जहाँ सामुदायिक/संस्कृति विशेष ज्ञान को अपनी व्यवस्था में शामिल करने से पहले उसका रूपांतरण व प्रसंस्करण होना अनिवार्य हो जाता है। बेड़िया समुदाय के चलायमान होने की जीवनशैली से उपजी संस्कृति उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं में परिलक्षित होगी। इस आधार पर सेक्सुअलिटी व उनके स्त्री-पुरुष संबंधों, उनके औपचारिक-अनौपचारिक व्यवहारों, यहां तक कि जीवन और नृत्य-गीतों की अल्हड़ता का अध्ययन और व्याख्या अपनी सम्पूर्णता में गैर विषयीकृत (Non Subjectifed) होकर ही संभव है।
----------------